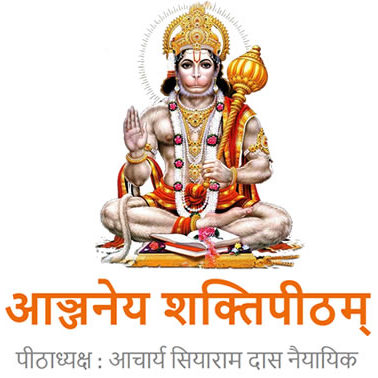ब्रह्मगायत्री मन्त्र का सप्रमाण विशद अर्थ
“ॐ भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् “
जप के पूर्ण फल को या इष्ट की असीम कृपा का भाजन बनने के लिए और जप के समय मन को अनेक कल्पनाओं से विरत करने का साधन मन्त्रार्थ चिन्तन है । हम व्याहृतियों के विषय में बतला चुके हैं ।
इस परम शक्तिमय गायत्री मन्त्र का अर्थ मैने अनेक लोगों के द्वारा लिखा देखा है । और उन पर व्यंगबाणों की बौछार भी । जिसका खण्डन आप सब मनीषी इससे पूर्व पोस्ट में देख चुके हैं ।
इस मन्त्र का “तत्” और “यो” तथा “भर्गो” शब्द विद्वत्कल्पों की जिज्ञासा के विषय बने रहे ।
आलोचकों का मुहतोड़ उत्तर दिया जा चुका है । उससे जिज्ञासुओं की जिज्ञासा का शमन भी हुआ होगा ।
पर कुछ अनभिज्ञों ने तो “भर्गो” की जगह “भर्गं” करने का दुस्साहस भी किया ; क्योंकि “भर्गं” उन्हे द्वितीया विभक्ति का रूप लगा और “भर्गो” प्रथमान्त पद ।
पहले हम भर्ग शब्द पर चर्चा करते हैं–
भर्ग शब्द हमारे सामने हिन्दी रूप में उपस्थित होता है और जब उसका संस्कृत रूप में प्रयोग करते हैं –”भर्गः” .
तब इसका अर्थ होता है–भगवान् शिव,
और संस्कृत व्याकरण के अनुसार यह भर्ग शब्द “भृज” धातु से “नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः” सूत्र से अच्
प्रत्यय तथा न्यंकादित्वात् ज को ग होकर बना है ।
“हलश्च” सूत्र से “घञ्” प्रत्यय करके भी भर्ग शब्द निष्पन्न होता है ।
यह हमारे सर्वोत्तम संस्कृतव्याकरण की महिमा है । जिसके समक्ष आज तक विश्व का कोई व्याकरण खड़ा ही नहीं
हो सका ।
इसलिए अमरकोष में — ” हरः स्मरहरो भर्गः ” इस प्रकार शिव जी के नामों में हरः के समान प्रथमान्त भर्गः शब्द का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है ।
किन्तु यह शब्द गायत्री मन्त्र में नहीं है ;क्योंकि “धीमहि” क्रिया का कर्म बनने के लिए इसे द्वितीयान्त “भर्गं” बनना पडेगा । जो कि मन्त्र के स्वरूप के अनुरूप नही है ।
दूसरा शब्द है “भर्गस्” सकारान्त । इसके विषय में पूर्व पोस्ट में हम विशेष विवेचन कर चुके हैं ।
इसका अर्थ है –ज्योति — दिव्यतेज ।
यह शब्द नपुंसक लिंग में है और इसका रूप यशस् शब्द की भांति –भर्गः भर्गसी भर्गांसि –ऐसा प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में चलता है ।
यही द्वितीया विभक्त्यन्त “भर्गः” शब्द देवस्य के पूर्व में होने के कारण भर्गो रूप में आया है –यह बात पहले पोस्ट
में स्पष्ट की जा चुकी है ।
धीमहि –यह शब्द ध्या धातु के लिङ् लकार का बहुवचन में छान्दस प्रयोग है । जिसका अर्थ है –ध्यायेमहि –हम सब ध्यान करते हैं ।
नः — यह शब्द “अस्मद्” शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप है । इसका वही अर्थ है जो “अस्माकं” शब्द का है । अर्थात्
हम लोगों की ।
मन्त्रार्थ
मन्त्र का अर्थ बतलाने के लिए उनमें आये हुए पदों को अर्थानुसार आगे पीछे जोड़ना पड़ता है जिसे “अन्वय” कहा
जाता है ।
अब अन्वय देखें–
“देवस्य सवितुः वरेण्यं तत् भर्गो धीमहि यो नः धियः प्रचोदयात्”
अब अर्थ देखें –
देवस्य –दिव धातु से अच् प्रत्यय करके देव शब्द बना है । दीव्यति –प्रकाशते इति देवः तस्य –जो प्रकाशमान है उसे देव कहते हैं, उनके ।
सवितुः– सु आग्रह करता हूं, प्रेरणार्थक षू धातु से तृच् प्रत्यय होकर सविता शब्द बना है । सुवति -प्रेरयति प्राणिनः स्वस्वकार्येषु इति सविता -सूर्यः, तस्य सवितुः –जो उदित होकर सम्पूर्ण प्राणियों को उनके उनके कार्यों को करने के लिए प्रेरणा देते हैं उन भगवान् सूर्य को हम “सविता” शब्द से कहते हैं । उन सूर्यसम्बन्धी । सवितुः में षष्ठी विभक्ति सम्बन्धार्थिका है । अर्थात् प्रकाशमान सूर्य देव से सम्बन्धित ।
वरेण्यं –वरण करने के योग्य अर्थात् सर्वश्रेष्ठ। वरणार्थक “वृञ्” धातु से “वृञ एण्यः ” -३/९८, इस औणादिक सूत्र से एण्य प्रत्यय और गुण आदि होकर “वरेण्यं” बना है ।
अमरकोष में इसे श्रेष्ठ के पर्यायों में गिना गया है ।-३/१/५७,
तत् –ब्रह्म अर्थात् भगवान् ,
” तत् ” शब्द को ब्रह्मवाचक ‘ भगवद्गीता में कहा गया है –
“ॐतत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः “
–१७/२३,
भर्गो–ज्योतिः–तेजःस्वरूप का ।
भगवान् को ज्योतिस्वरूप वेदों तथा संहितादि ग्रन्थों में कहा गया है । —
“यत्परं यद्गुणातीतं यज्ज्योतिरमलं शिवम् ।
तदेव परमं तत्त्वं कैवल्यपदकारणम् । ।
श्रीरामेति-।”
“परं ज्योतिरुपसम्पद्य”–छान्दोग्य-८/१२/२,
इन प्रमाणों से भगवान् भास्कर से सम्बद्ध जो ब्रह्म तत्त्व है वह ज्योतिस्वरूप है ,गुणातीत है उसे श्रीराम,कृष्ण, शिव, नारायण आदि किसी भी नाम से कहें–इसमें आप अपनी निष्ठा के अनुसार स्वतन्त्र हैं ।
ध्यातव्य है कि इस ब्रह्म तत्त्व का ध्यान सूर्यमण्डल के अन्दर करना है । यही अर्थ सूर्यसम्बन्धी ज्योतिस्स्वरूप ब्रह्म से अभिप्रेत है ।
अत एव गायत्रीजपाधिकार में महर्षि मार्कण्डेय कहते हैं –
” अर्कमध्यगतं ध्यायेत् पुरुषं तु महाद्युतिम् ।
—स्मृतिचन्द्रिका,आह्निककाण्ड-गायत्रीजपविधिः
–सूर्यमण्डल के मध्य परम प्रकाशयुक्त पुरुष का ध्यान करना चाहिए ।
“सूर्यमण्डलमध्यस्थं रामं सीतासमन्वितम् ।
नमामि पुण्डरीकाक्षं–.”
–सनत्कुमारसंहिता ,रामस्तवराज
यहां गायत्री माँ के ध्यानकर्ता घबड़ायें नहीं ;क्योंकि सम्पूर्ण चराचर में निवास करने के कारण “पूर्षु -सर्वशरीरेषु शेते इति पुरुषः” व्युत्पत्ति उन माँ में पूर्णतया घटित हो रही है ।
धीमहि –हम सब ध्यान करें अर्थात् ध्यान करते हैं ।
यहां बहुवचन की क्रिया “धीमहि” से २ प्रकार का संकेत मिलता है –
१–कई साधक एक साथ बैठकर साधना करें तो इस मन्त्र का आभामण्डल शीघ्र ही फैलकर विश्वकल्याण करने लगेगा ।
२–यदि साधक अकेले जप कर रहा है तो बहुवचन का तात्पर्य यह है कि वह केवल अपने लिए ही नही अपितु अपने सभी सम्बन्धियों की ओर से ध्यान कर रहा है ।
“यह इस ब्रह्मगायत्री की एक प्रमुख विशेषता है । एक से अनेक का कल्याण” .
यो–जिन परमात्मा का हम ध्यान कर रहे हैं अर्थात् जो हमारे ध्येय हैं वे ।
नः-हम सबकी । धियो –बुद्धियों को । प्रचोदयात् –अच्छे कर्मों में प्रेरित करें । यह प्रेरणार्थक चुद् धातु के लिङ् लकार
का रूप है ।
यहां भी “नः” और “धियो” में बहुवचन का यही तात्पर्य है कि गायत्री महामन्त्र का अनुष्ठाता केवल अपना ही नहीं अपितु अपने सभी सम्बन्धियों का कल्याण अनायास कर देता है ।
अतः इस महामन्त्र के अर्थ का अनुसन्धान करके जप का पूर्णरूपेण लाभ लेना चाहिए ।
जय श्रीराम
#आचार्यसियारामदासनैयायिक

Gaurav Sharma, Haridwar