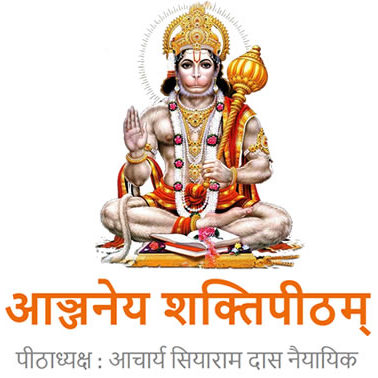अर्जुन उवाच
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ।इषुभि: प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ॥४॥
व्याख्या – पूर्व में अर्जुन ने कहा था कि इस युद्ध में स्वजनों के वध से हमें नरक की प्राप्ति होगी; क्योंकि हमें इनके वध से पाप लगेगा—“पापमेवाश्रयेदस्मान्—“१/३६, मधुसूदन ! हम शोक या मोह के वशीभूत होकर युद्धरूपी स्वधर्म का त्याग नहीं कर रहे हैं अपितु पाप के भय से हम युद्ध नहीं करना चाहते । इसी तथ्य का निरूपण स्वयं पार्थ द्वारा किया जा रहा हैं—कथमित्यादि पदकदम्बों से ।
भीष्मं= पितामह भीष्म, और ,द्रोणं=आचार्य द्रोण को, संख्ये= युद्ध में, इषुभि:= बाणों से, कथं= कैसे, प्रतियोत्स्यामि= मारूंगा ? अर्थात् किसी भी प्रकार मैं उन्हें नहीं मार सकता ।क्यों ? क्योंकि वे दोनों, पूजार्हौ= पुष्पादि से पूजा के योग्य हैं न कि भयंकर बाणों से वध के योग्य । मधुसुदन= मधु जैसे दुष्ट दैत्य के निहन्ता ! अर्जुन मधुसूदन सम्बोधन से यह ध्वनित कर रहे हैं कि आप दुष्टदैत्यों के प्राणहर्ता हैं ।ऐसे आप मुझे पूज्यों के वध में क्यों प्रेरित कर रहे हैं ?
मधुसूदन और अरिसूदन इन दो सम्बोधनों का प्रयोग प्रभु के लिए पार्थ द्वारा हुआ है । मधुसूदन सरस्वतीपाद कहते हैं कि शोकाकुल अर्जुन को पूर्वापर के परामर्श का वैकल्य होने से ऐसा हुआ है ।शोक से व्याकुल पुरुष को ्यान नहीं रहता इसलिए वह ऐसा कह देता है । फलत: यह पुनरुक्त दोष नहीं है ।
विचार करें तो मधुसूदन सम्बोधन द्रोणं च के साथ सम्बद्ध है और अरिसूदन पूजार्हौ के साथ । अर्जुन मधुसूदन सम्बोधन से यह कहना चाहते हैं कि आप देव हैं और आपने विजातीय दुष्ट मधु दैत्य का वध किया है । किन्तु मुझे अपने सजातीय सज्जन पितामह भीष्म और उनके भी पूज्य आचार्य द्रोण का वध करने को कह रहे हैं ।
पूजार्हौ अरिसूदन । शत्रुओं का विनाश करने वाले ! इसका पूजार्हौ के साथ सम्बन्ध है । आप रिपुओं का नाश करते हैं और मुझे पूजा करने योग्य अर्थात् शत्रुभाव से विनिर्मुक्त महापुरुषों के विध्वंस हेतु प्रेरित कर रहे हैं । क्या यह उचित है ??
इसलिए पार्थ के द्वारा प्रयुक्त सम्बोधनद्वय विलक्षण भाव को प्रस्तुत करने से सार्थक हैं । फलत: पौनरुक्त्य नहीं ।
पूजार्हौ । वे दोनों पूजा के योग्य हैं । अपूज्य की पूजा और पूज्य की अपूजा दोनों ही अधर्म है । पूज्य की पूजा तथा अपूज्य की अपूजा ये दोनों धर्म हैं । जैसे पूज्य की पूजा विहित होने से धर्म है वैसे ही उनके साथ युद्ध करना महा अधर्म है । यदि कहें कि पूज्यों के साथ युद्ध निषिद्ध न होने से अधर्म नहीं है तो इसका उत्तर सुनें —
गुरुं हुंकृत्य त्वंकृत्य विप्रं निर्जित्य वादत: । श्मशाने जायते वृक्ष: कंकगृद्धोपसेवित:॥
गुरु को हुंकार अथवा त्वम् तुम इस प्रकार अपमानसूचक शब्दों से बोलने वाला तथा ब्राह्मण को वाद में जीतता है । वह श्मशान में कौआ और गीध से सेवित वृक्ष बनता है । ( यद्यपि वाद उस वार्तालाप को कहते हैं जिसे तत्त्व को जानने की इच्छा से आरम्भ किया जाता है—“ तत्त्वबुभुत्सो: कथा वाद:” । अतएव श्रेष्ठ होने से इसे भगवान् ने गीता में “वादः प्रवदतामहम्॥” से अपनी विभूति में परिगणित किया ।तथापि मध्य में विजिगीषा से यदि प्रश्न आदि करके विप्र पर विजय पायी जाय तो जीतने वाला नरकतुल्य कष्ट अवश्य भोगता है । अथवा कुछ लोगों ने वाद के दो भेद स्वीकार किया है । प्रथम जल्प, द्वितीय वितण्डा । जैसे— तत्र वादो नाम य: परस्परेण सह शास्त्रपूर्वकं विगृह्य कतयति । स वादो द्विविध:संग्रहेण जल्पो वितण्डा च . तत्र पक्षाश्रितयोर्वचनं जल्प: । जल्पविपर्ययो वितण्डा ॥-इति चरके विमानस्थानेSष्टमेSध्याये )
प्रत्येक स्थिति में जीतने की इच्छा से चलने वाला वार्तालाप तत्त्वनिरूपणफलक न होकर परप्रतिष्ठा का विघातक होने से निक़ृष्ट फल नरकादि देने वाला है । वस्तुत: “उद्यते कथ्यते छलपूर्वकमसौ अशास्त्रीय: पक्ष:
इति वाद: । इस प्रकार यौगिक व्युत्पत्ति से छलपूर्वक असत् पक्ष का कथन यहां वाद पद से अभीष्ट है । अन्यथा शास्त्ररक्षा एवं वैदिक सनातन धर्म की सुरक्षा हेतु नास्तिक ब्राह्मणको पराजित करने पर भी नरकादि की प्रसक्ति होगी । अशास्त्रीय पक्ष का प्रतिपादन शास्त्रीय पक्ष का खण्डन ये दोनों विप्र के लिए निरयप्रद हैं ।
जब गुरु के प्रति हुंकार और त्वंकार जैसे शब्दप्रयोग नरकप्रद होते हैं तब साक्षात् वज्रवत् बाणों का प्रयोग निरयप्रद क्यों नहीं होगा ?? अत एव मैं इनके साथ अधर्मात्मक युद्ध नहीं कर सकता ।
—जय श्रीराम—
#आचार्यसियारामदासनैयायिक

Gaurav Sharma, Haridwar