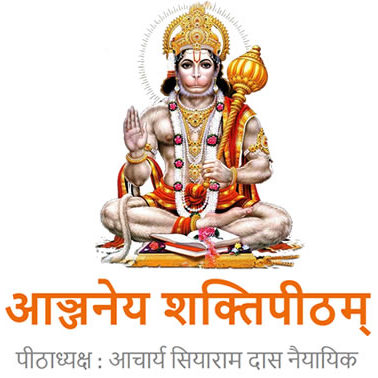अर्थवाद –जिन वाक्यों के द्वारा विधेय वस्तु की स्तुति की जाती है | उन्हें अर्थवाद कहा जाता है | ये वाक्य ३ प्रकार के होए हैं –
१-गुणवाद, २-अनुवाद, ३-भूतार्थवाद ( यथार्थवाद )|
१-गुणवाद—गुणवाद रुपी अर्थवाद वे वाक्य हैं जिनके द्वारा कहे गए अर्थ का प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध है | जैसे—होम की प्रशंसा करने के लिए तैत्तिरीय संहिता में वाक्य आया—“ स आत्मनो वपामुदक्खिदत्तामग्नौ प्रागृह्णात् ”—२/१/१, ( प्रजापति ने अपनी वपा को निकालकर अग्नि में आहुति दे दी )—इस वाक्य से जो अर्थ बतलाया जा रहा है,वह प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी वपा को शरीर से निकालकर जीवित नही रह सकता | अतः इस प्रकार के जो भी वाक्य हैं उन्हें गुणवादरूप अर्थवाद समझना चाहिए |
२-अनुवाद- अनुवादात्मक अर्थवाद वे वाक्य है जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध अर्थ को बतलाते हैं | जैसे—“वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता—” ( वायु शीघ्र चलने वाली देवता है )—यहाँ जो वायु में शीघ्रगामित्व बतलाया जा रहा है |वह प्रत्यक्ष प्रमाण से हम सभी जानते हैं | अतः प्रत्यक्ष से सिद्ध अर्थ को बतलाने वाला यह वाक्य उसका अनुवादक मात्र माना गया है | इस प्रकार के सभी वाक्य अनुवाद रूप अर्थवाद की श्रेणी में रखे गए हैं |
३—भूतार्थवाद—भूतार्थवाद उन वाक्यों को कहते हैं जिनके द्वारा कथित अर्थ को प्रत्यक्षादि प्रमाणों से न तो झुठलाया जा सकता है और न ही सिद्ध किया जा सकता | जैसे—“ इन्द्रो वृत्रमहन् ”-( इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया ) इस अतीत वृत्रवध रूप अर्थ को हम प्रत्यक्षादि प्रमाणों से न तो झुठला सकते हैं और न ही उसे सिद्ध कर सकते | तात्पर्य यह कि जहाँ प्रत्यक्षादि प्रमाणों की गति नही है उन अर्थों के बोधक वाक्य यथार्थवाद रुपी अर्थवाद कहे जाते हैं, इन्हे ही भूतार्थवाद कहा गया है |
पूर्वमीमांसा में यह श्लोक अति प्रसिद्ध है—
“विरोधे गुणवादः स्यादनुवादोSवधारिते | भूतार्थवादस्तद्धानादर्थवादस्त्रिधा मतः ||
—जय श्रीराम-
–जयतु भारतम्, जयतु वैदिकी संस्कृतिः-
-#आचार्यसियारामदासनैयायिक—